भारतीय संस्कृति की अवधारणा : आश्रम व्यवस्था
भारतीय संस्कृति की अवधारणा 01
आश्रम व्यवस्था के बारे में जानकारी
- भारतीय संस्कृति में सम्पूर्ण जीवनकाल को व्यवस्थित करने के लिए आश्रम व्यवस्था के रूप में नियोजित किया गया है। जीवन के सभी शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक-व्यावहारिक तथा अध्यात्मिक आयामों का विकास किया जा सके, इसलिए ऋषियों ने आश्रम व्यवस्था का निर्धारण किया था । मनुष्य अपनी आयु के विभिन्न पड़ावों पर भिन्न-भिन्न उत्तरदायित्वों का निर्वहन करते हुए अंतिम लक्ष्य मोक्ष को प्राप्त कर सके। इस व्यवस्था के अन्तर्गत जीवन की आयु को 100 वर्ष मानकर इसे चार आश्रमों में बांटा गया है और प्रत्येक आश्रम से सम्बन्धित व्यक्ति के दायित्वों एवं कर्तव्यों का निर्धारण किया गया है।
- प्रथम पच्चीस वर्ष शरीर, मन और बुद्धि के विकास के लिए निर्धारित किया गया है जिसे ब्रह्मचर्य आश्रम कहा गया है।
- द्वितीय पच्चीस वर्ष गृहस्थ आश्रम के लिए समर्पित किये गए हैं, जिसमें पति-पत्नी के रूप में धार्मिक जीवन व्यतीत करते हुए अपने नागरिक कर्तव्यों का पालन करते हुए जीवन यापन किया जाता है।
- तीसरे पच्चीस वर्ष गृहस्थ जीवन से मुक्त होकर पारमार्थिक जीवन जीने के लिए वानप्रस्थ आश्रम ग्रहण कर लिया जाता है। जीवन के अन्तिम पच्चीस वर्ष मोक्ष प्राप्ति के लिए संन्यास आश्रम में प्रवेश कर जाते हैं।
- चारों पुरुषार्थों का भी इन चार आश्रमों से घनिष्टतम सम्बन्ध है। आश्रमों के माध्यम से चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति सम्भव होती है। ब्रह्मचर्य आश्रम से मनुष्य धर्म के तत्वों को जानकर ज्ञानी बनता है। गृहस्थ आश्रम में उसी ज्ञान के प्रयोग से अर्थ व काम प्राप्त करता है, और मानव के सदाचरण के नियमों का पालन करता हुआ ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ तथा संन्यासी तीनों आश्रमों का पालन करने का दायित्व भी निर्वाह करता है। वानप्रस्थ आश्रम समाज सेवा के लिए रखा गया है। संन्यास आश्रम में मोक्ष प्राप्ति की साधना की जाती है। अतः चारों आश्रम व्यक्ति के चारों पुरुषार्थों को प्राप्त करने में मुख्य भूमिका निभाते हैं।
- ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ एवं संन्यास आश्रम के विषय में विस्तार से जानने के लिए आइये क्रमशः इन पर दृष्टि डालते हैं।
1 ब्रह्मचर्य आश्रम
- ब्रह्मचर्य आश्रम मानव जीवन का प्रथम सोपान है। प्राचीन काल में उपनयन संस्कार के साथ ही यह आश्रम प्रारंभ हो जाता था। इस आश्रम के अन्तर्गत गुरू बालक को अपने शिष्य के रूप में स्वीकार करके अपने आश्रम में रखकर विभिन्न विद्याओं में पारंगत करने का दायित्व निभाते थे। इस आश्रम में बालक ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए गुरु से शिक्षा ग्रहण करता था।
- ब्रह्मचर्य आश्रम में रहते हुए ब्रह्मचारी का मुख्य कर्म है कि अपने गुरु से विभिन्न शास्त्रों का ज्ञान एवं समस्त विद्याओं का प्रशिक्षण प्राप्त करे। इन विद्याओं का ज्ञान एवं प्रशिक्षण भौतिक संसार में उन्नति, बाधाओं से निपटने और संभावनाओं को साकार करने के लिए तथा पराभौतिक व्यक्तियों एवं आध्यात्मिक उन्नति से सम्बन्धित भी होता था।
- इस आश्रम में ब्रह्मचारी का समग्र विकास हो सके, इस बात का ध्यान रखा जाता था। शारीरिक विकास के लिए खेलों, व्यायामशालाओं का प्रचलन था। सामाजिक एवं व्यावहारिक ज्ञान के लिए कथानकों एवं घटनाओं का सहारा लिया जाता था। धर्मानुसार आचरण करना, नीति, नियमों का पालन करना आदि सीखता था। मानसिक विकास एवं आध्यात्मिक विकास के लिए आसन-प्राणायाम और ध्यान का अभ्यास कराया जाता था। इस आश्रम में ब्रह्मचारी का प्रमुख धर्म गुरु की सेवा, गुरु की कृपा प्राप्त करना होता था। पच्चीस वर्ष की आयु तक शेष जीवन जीने की योग्यता प्राप्त कर अगले गृहस्थ आश्रम की ओर प्रस्थान करता था। आधुनिक शिक्षण व्यवस्था में गुरु-शिष्य का सम्बन्ध इस प्रकार का नहीं रहने के कारण समाज में अच्छे नागरिक नहीं मिल रहे हैं।
2 गृहस्थ आश्रम
- प्रारंभिक ब्रह्मचर्य आश्रम का जीवन पूर्ण करने के बाद व्यक्ति गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता है। चारों आश्रमों में गृहस्थ आश्रम को सबसे अधिक महत्वपूर्ण एवं श्रेष्ठ माना गया है। क्योंकि इस आश्रम में रहकर परिवार, समाज, राष्ट्र की सेवा करने का अवसर प्राप्त होता है। ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ तथा संन्यास आश्रम में रह रहे लोगों के भोजन, वस्त्र एवं अन्य आवश्यक सामग्री गृहस्थों से ही प्राप्त होती है।
- गृहस्थ आश्रम में प्रवेश आचार्य की अनुमति मिलने के बाद ही होता था। जब आचार्य यह समझ लेते थे कि ब्रह्मचारी गृहस्थ धर्म के पालन में सक्षम है, तभी उसको अगले गृहस्थ में प्रवेश की आज्ञा मिल जाती थी। स्त्री-पुरुष के बीच विवाह संस्कार के साथ साथ ही एक दम्पत्ति के रूप में गृहस्थ आश्रम प्रारम्भ हो जाता है। विवाह का उद्देश्य यौन संतुष्टि और सन्तानोत्पत्ति होता है। सन्तान उत्पत्ति से समाज सन्तुलन और निरन्तरता बनी रहती है। गृहस्थ आश्रम में रहकर मनुष्य ऋणों से मुक्त होने के उपाय भी करता है। होम, यज्ञादि से देव ऋण से मुक्त होता है। वेद मंत्रों के यूनिटन, जपादि से ऋषि ऋण से मुक्ति प्राप्त होती है। माता-पिता की सेवा, व विधानयुक्त उनके अंतिम संस्कार से पितृ ऋण से मुक्ति मिलती है। अतिथियों की सेवा, पशु-पक्षियों के लिए अन्न-जल का प्रबन्ध करना, वृक्षारोपण, नदियों का पूजन भी समाज-वातावरण के भार से मुक्त करता है।
3 वानप्रस्थ आश्रम
- वानप्रस्थ आश्रम इस व्यवस्था का तीसरा महत्वपूर्ण आश्रम है। गृहस्थ आश्रम में रहकर विधिवत् धर्म का पालन करके जब गृहस्थ यह देखे कि उसके बाल श्वेत होने लगे हैं, और उसके पुत्र का भी पुत्र हो गया हो तो उस व्यक्ति को वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश करना चाहिए। इस आश्रम का पालन करने के लिए व्यक्ति अपने निकट सम्बन्धियों से अलग होकर एकान्तवास के लिए वन की ओर प्रस्थान करता है। पत्नी को अपने पुत्रों के संरक्षण में या अपने साथ भी रख सकते हैं।
- वानप्रस्थ आश्रम में व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं को सीमित करके तपस्या से युक्त जीवन-यापन करता है। इस आश्रम में सांसारिक मोह-माया से विमुख होकर व्यक्ति निष्काम कर्म में लग जाता है। वानप्रस्थ आश्रम में व्यक्ति आश्रमों में गुरु का दायित्व निर्वहन करता है तथा विद्यार्थियों के ज्ञान-विद्यादि के शिक्षण-प्रशिक्षण के महत्वपूर्ण कार्यों में संलग्न हो जाता है। इस आश्रम में रहकर व्यक्ति को मानसिक रूप से संन्यास आश्रम के लिए अपने आपको तैयार करना होता है।
4 संन्यास आश्रम
- आयु के अन्तिम पड़ाव में संन्यास ग्रहण करने का विधान किया गया था। आश्रम व्यवस्था में संन्यास आश्रम चतुर्थ और अन्तिम आश्रम है। संन्यास शब्द का सामान्य अर्थ है त्यागना, या त्याग कर देना । मनुष्य जब सांसारिक भोगों, इच्छाओं और फलों का त्याग कर देता है, तब वह संन्यासी हो जाता है। पिछले तीनों आश्रमों के बाद संन्यास आश्रम प्रारम्भ हो जाता है। संन्यास आश्रम में प्रवेश का वही अधिकारी माना गया है जिसने अपने पिछले तीनों आश्रमों में रहकर अपने कर्तव्यों का पालन कर लिया हो। वह तीनों ऋणों से मुक्त हो जाता है। इसलिए यज्ञोपवीत धारण नहीं करता।
- संन्यासी सांसारिक सुखों का परित्याग कर देता है। उसके पास कोई घर, सम्पत्ति आदि नहीं होती है। वह भिक्षा से प्राप्त अन्न, वस्त्रादि ग्रहण करता है। वर्षा ऋतु में एक ही स्थान पर रहकर समय व्यतीत करता है तथा अन्य ऋतुओं में भ्रमणशील होकर रहता है। संन्यासी गेरुए वस्त्र धारण करता है। भिक्षा पात्र, दण्ड और कमण्डल लेकर विचरण करता है।
- संन्यासी मोक्ष प्राप्ति के निमित्त मोह-माया, स्नेह, घृणा, प्रेम, द्वेष आदि से सदा ऊपर उठ जाता है। व्यक्ति इस आश्रम में मोक्ष प्राप्ति की साधना में निमग्न होकर उसे प्राप्त करता है।


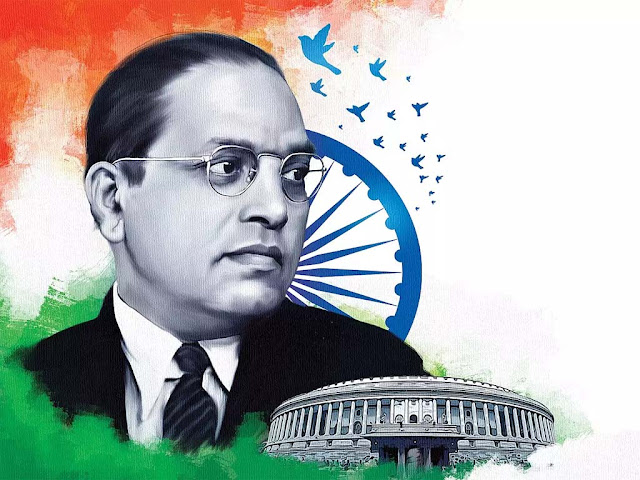
Post a Comment